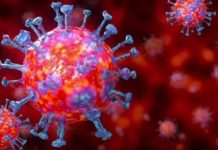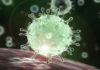किसानों के आंदोलन को 81 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। आरोप-प्रत्यारोप को एक तरफ रख दें तो आंदोलन कमोबेश गैर-राजनीतिक है और गांव के लोगों के हाथ में है। हालांकि ठीक से देखने पर यह इसकी कमी ही मानी जाएगी कि शहर के लोगों का समर्थन हासिल करने में इसे खास सफलता नहीं मिल पाई है। आंदोलन शहरी जनता को समझा नहीं पाया है कि इसकी मांगें देश की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी हैं। लेकिन जगह-जगह आयोजित हो रही किसान महापंचायतों के जरिए इसने ग्रामीण जनता के हर तबके का समर्थन जुटाया है। भावनात्मक मुद्दों से अलग जीवन के बुनियादी मसलों पर लोगों को इकट्ठा करने का यह अभियान लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
कांटे के बदले फूल
गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद से संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं, खासकर राकेश टिकैत ने अहिंसक आंदोलन के लिए जरूरी सावधानियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की सीमाओं पर भारी पुलिस बंदोबस्त और कील भरे अवरोधों से उपजे तनाव को कम करने के लिए उन्होंने फूल बोने का प्रतीकात्मक कार्यक्रम किया तथा छह फरवरी के चक्का जाम में उपद्रव की साजिश रची जाने की सूचना मिलने पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इससे मुक्त रखा। इनसे अलग किसान आंदोलन की मांगों तथा इसके स्वरूप पर नजर डालें तो कई तरह के सवाल उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या यह आंदोलन खेती तथा इससे जुड़े लोगों की हालत में लगातार आ रही गिरावट को रोकने में कामयाब हो पाएगा? यह पूरा मामला क्या आंदोलन के अजेंडे पर आ सका है?
ऐसा नहीं है कि किसान कोई पहली बार खड़े हुए हैं। आज अगर किसान इस आंदोलन को भारी संख्या में समर्थन दे रहे हैं तो इसमें पिछले आंदोलनों से आई जागरूकता का बड़ा योगदान है। लेकिन क्या यह आंदोलन खेती के संकट, खासकर दुनिया में खड़ी की गई अर्थव्यवस्था में खेती के स्थान के सवाल को हल करने का कोई खाका पेश कर पा रहा है? आंदोलन का सारा ध्यान तीन कानूनों को रद्द कराने के तात्कालिक उद्देश्य पर टिका है। जरूरी है कि इस बड़े आंदोलन की ऊर्जा खेती-किसानी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े उन सवालों को हल करने में भी लगाई जाए जो अब असाध्य बीमारी का रूप ले चुके हैं। खेती के संकट की चर्चा करते समय आंकड़ों में गए बगैर भी हम कुछ बातें पक्के तौर पर कह सकते हैं। सबसे बड़ा तथ्य तो यह है कि देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा खेती पर आश्रित है। इस तथ्य का भी अलग से सत्यापन जरूरी नहीं है कि आबादी का यही हिस्सा सबसे गरीब है।
गरीबी से छुटकारा पाने के लिए गांव से शहर आए ये लोग ही शहरों की गरीब आबादी का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि खेती उन्हें रोजगार नहीं दे पाती और शहर उन्हें जीने लायक जिंदगी नहीं दे पाते। गांवों से शहर आ रहे लोगों को ‘पलायन’ शब्द पूरा न्याय नहीं दे पाता है। इसे हांका जैसा कोई नाम देना चाहिए जो उस क्रूरता को जाहिर कर सके जो लोगों के इस आने-जाने में गुंथी है। कोरोना महामारी में पलायन के पीछे छिपी यह क्रूरता सामने आई थी। प्रवासी मजदूरों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था और शहर की स्वास्थ्य या दूसरी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल सकती थीं। इससे यह भी पता चलता है कि ये लोग अवसर की तलाश में शहर नहीं आए थे। कृषि में घाटा यहां तक पहुंच गया है कि यह गांव की बड़ी आबादी को शहर की ओर फेंक देता है।
खेती में घाटे के कारण हो रही आत्महत्याएं पहले अखबार की सुर्खियां बनती थीं, लेकिन अब यह इतनी सामान्य सी बात हो गई है कि इसकी चर्चा भी बंद हो गई है। बैंकों की कर्ज प्रणाली में सुधार, कर्ज की माफी तथा अनुदान आदि भी इन्हें रोक नहीं पाए। किसानों को लग रहा है कि नए कानून गांव की बची-खुची अर्थव्यवस्था को भी नष्ट कर देंगे। सरकार इस संदेह को दूर नहीं कर पा रही है। असल में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनी पिछली नीतियों से गांव के लोगों का कष्ट दूर नहीं हुआ है और किसानों को नए कानून भी उन्हीं नीतियों की तरह दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये कानून खेती के घाटे को कम करने के बदले खेती पर किसानों के नियंत्रण को ही कमजोर कर देंगे। उनकी मांग का मूल यही है कि खेती पर उनका नियंत्रण रहे और घाटे को पूरा करने के लिए समर्थन मूल्य मिलने की कानूनी व्यवस्था हो। लेकिन क्या इतने भर से खेती का संकट दूर हो जाएगा?
इसका उत्तर नकारात्मक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट समर्थन-मूल्य की गारंटी भर से हल नहीं हो सकता है। यह एक तात्कालिक उपाय ही है। खेती के संकट औद्योगिक सभ्यता ने पैदा किए हैं। इस सभ्यता के स्वरूप की व्याख्या गांधी जी ने सौ साल पहले की थी। उन्होंने आगाह किया था कि पृथ्वी अपने समस्त वासियों की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन उनके लालच को पूरा नहीं कर सकती।
गांव के कुटीर उद्योग
चौड़ी सड़कों, बड़ी बिजली परियोजनाओं तथा कारखानों के लिए हम खेती और जंगल की जमीन को खत्म कर रहे हैं। इससे गांव के कुटीर उद्योग भी नष्ट हो रहे हैं। स्वचालित मशीनों तथा खाद ने खेती के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। रोजगार खत्म हो रहे हैं। इस आंदोलन को इन दीर्घकालिक मुद्दों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मछुआरों का आंदोलन चलाने वाले अनिल प्रकाश जैसे कुछ विचारक यह सुझाव दे रहे हैं कि मछली और भेड़ आदि पालने वालों को भी किसान माना जाए। इस पर विचार होना चाहिए। हमारे समाज में संवाद की जगह धीरे-धीरे कम हो रही है। किसान आंदोलन लोकतंत्र की इस जरूरी पहचान को पूरी तरह अपनाकर चले तो न केवल अपना दायरा बढ़ाएगा बल्कि व्यवस्था को मानवीय बनाने और खेती से जुड़े अहम सवालों को केंद्र में लाने में भी सफल हो सकता है।
अनिल सिन्हा
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके निजी विचार हैं)