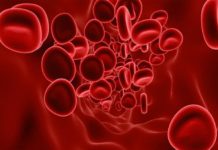चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सौ साल पूरे कर रही है। चीन में इस मौके पर एक जुलाई को होने वाले शानदार जश्न की तैयारियां काफी पहले से चल रही हैं। यह स्वाभाविक भी है। 1949 में हुई क्रांति के बाद से चीन में इसी पार्टी का शासन है। इसी के नेतृत्व में चीन कृषि प्रधान देश से औद्योगिक राष्ट्र में तब्दील होते हुए आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सबसे बड़ी बात यह कि इतना सब करके भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी थकी हुई नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं लग रहा कि उसे बाहर या अंदर से कोई बड़ा खतरा है। खतरे की बात इसलिए अहम है क्योंकि हम देख चुके हैं कि पिछली सदी के आखिरी दशक में संसार का दूसरा सुपर पावर माना जाने वाला सोवियत संघ और उसके साथ पूरा सोशलिस्ट ब्लॉक कैसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने आप ढह गया। दुनिया भर में इसे ठीक ही वामपंथ की घोर विफलता माना गया।
कुछ बुनियादी सवाल
यह सवाल हर विचारशील व्यक्ति के मन में है कि आखिर क्या बात है कि जो विचारधारा सोवियत संघ समेत दुनिया के ज्यादातर देशों के पांवों की जंजीर साबित हुई, वही चीन को तरक्की की राह पर सरपट दौड़ाए चली जा रही है? इसलिए यह और जरूरी हो जाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इन सौ सालों की रोशनी में वामपंथ से जुड़े कुछ बुनियादी सवालों पर विचार किया जाए तो वामपंथ की बुनियादी कसौटियों के आलोक में उन बड़े दावों को भी परखा जाए, जो कम्युनिस्ट पार्टियां विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने करती रही हैं।
इसमें कोई शक नहीं है कि 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुआई में महज सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था, वह क्रांति थी। यानी उस परिघटना में सत्तारूढ़ वर्ग को उखाड़ कर अन्य वर्ग ने सत्ता पर कब्जा किया था। लेकिन वह सर्वहारा क्रांति नहीं थी। उस क्रांति से सत्ता पर मजदूर वर्ग का कब्जा नहीं हुआ था। खुद माओ ने उसे नव-जनवादी क्रांति कहा था। मतलब यह कि उस समय तक जिसे जनवादी क्रांति कहा जाता था, यह उससे अलग कोई चीज थी, इसमें कुछ नयापन था। वह नयापन क्या था? नई बात उसमें यह थी कि उस क्रांति में माओ ने चार वर्गों को शामिल बताया था। मजदूर और किसान के अलावा उसमें पूंजीपति वर्ग का एक हिस्सा भी शामिल था, जिसे माओ ने राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के रूप में परिभाषित किया था।
क्रांति के बाद भूमि सुधार के जो बड़े कदम उठाए गए थे, उनसे भी इस बात की पुष्टि होती है कि जनवादी क्रांति अपने कार्यभार को पूरा कर रही थी। लेकिन मूल सवाल तो यह है कि जब 1949 में मजदूर वर्ग के बजाय पूंजीपति वर्ग सत्ता में आया, तो फिर उसके बाद वहां दूसरी क्रांति कब हुई जिसमें मजदूर वर्ग ने पूंजीपति वर्ग को बेदखल कर सत्ता पर कब्जा किया? रूस में मार्च 1917 में हुई जनवादी क्रांति के बाद नवंबर में सर्वहारा क्रांति हुई मानी गई। चीन में ऐसा कब हुआ? कुछ लोग इसका जवाब सांस्कृतिक क्रांति में तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे जितनी भी छोटी या बड़ी रही हो, चाहे जितनी भी विफल या सफल रही हो, थी तो वह सांस्कृतिक क्रांति ही। तो क्या सांस्कृतिक क्रांति से राजनीतिक क्रांति का कार्यभार पूरा हो सकता है? अगर हां तो फिर राजनीतिक क्रांति की जरूरत ही क्या थी? दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन सांस्कृतिक क्रांति से ही काम चला लेता। लेकिन अगर नहीं तो यह मानना होगा कि चीन में वह कार्यभार अधूरा ही रहा। जितने तरह की उथल-पुथल और नीतियों में जो बड़े बदलाव हम वहां देखते हैं, वे पूंजी के ही अलग-अलग रूपों के टकराव की झलक थे, चाहे वह कृषि पूंजी और औद्योगिक पूंजी का टकराव हो या फिर औद्योगिक पूंजी और वित्त पूंजी का।
यही वजह है कि चीन सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा और प्रतिबद्धता के बारे में चाहे जो भी दावे करती रही हों, पूंजी के तर्क को शिरोधार्य करते हुए चलने वाले तमाम देशों, कंपनियों और संस्थाओं को चीन की मौजूदगी से वैसी असुविधा नहीं होती जैसी किसी जमाने में सोवियत संघ का नाम भर सुन लेने से होने लगती थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन में भी चीन 2001 में ही आ गया और पिछले दो दशकों से बिना किसी खास कठिनाई के इसमें बना हुआ है। अमेरिका समेत तमाम देशों से उसका टकराव पूंजी और श्रम के मूल तर्कों का टकराव नहीं बल्कि पूंजी के तर्क के मुताबिक होने वाला सामान्य टकराव ही है।
कथनी और करनी का फर्क
एकबारगी ऐसा लग सकता है कि कोई देश इतने लंबे समय तक कथनी और करनी का ऐसा फर्क कैसे चलाए रख सकता है। लेकिन यह वामपंथी आंदोलन की सामान्य बीमारी रही है और संभवत: उसके पतन का सबसे बड़ा कारण भी यही है। सच को सच कहने और डंके की चोट पर स्वीकार करने का मौजूदा संदर्भों में सबसे बड़ा उदाहरण लेनिन का माना जा सकता है। नवंबर 1917 की सर्वहारा क्रांति के चार साल के भीतर रूस में जो न्यू इकॉनमिक पॉलिसी लाई गई, उसके बारे में लेनिन ने खुद साफ-साफ कहा कि इसे समाजवाद की ओर बढ़ा हुआ कदम हर्गिज न माना जाए। यह पूंजीवाद से समझौता है, जो हम कुछ समय के लिए कर रहे हैं…। इसके बाद ऐसी साफगोई नहीं दिखती। चाहे दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान दुनिया के मजदूरों की नुमाइंदगी के सवाल को ताक पर रखने की बात हो या खुश्चेव के दौर में ‘शांतिपूर्ण सह अस्तित्व’ के सिद्धांत को स्वीकारने का, हर फैसला समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ाया गया कदम ही बताया गया। सबसे बड़ी बात कि विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन लगभग सर्वसम्मति से उसे स्वीकार भी करता रहा। वरना सोवियत संघ का पतन दुनिया भर के कम्युनिस्टों के लिए इतना तगड़ा भावनात्मक झटका नहीं होता।
प्रणव प्रियदर्शी
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं ये उनके निजी विचार हैं)