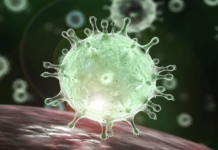आपने मुर्गों को लड़ते लड़ाते देखा है। कबूतर, कौए से लेकर शेर हाथी को लड़ते देखा होगा। सामान्यत: घोड़ों को लड़ते कम देखा जाता है। हां चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में घोड़ों को भीषण खून खराबे वाली लड़ाई का प्रदर्शन करके कमाई की जाती रही है। कई देशों में पशुओं को लड़ाने के कथित खेलों पर अब प्रतिबन्ध लग चुके हैं। लड़ाई से किसी को या मिला है और मिलेगा। लेकिन इन दिनों समाज, देश दुनिया को शांति सदभावना का संदेश देने वाले कुछ टीवी मीडिया चैनल, संपादक या स्वतंत्र रूप से सोशल मीडिया पर सक्रिय पूर्व संपादक, पत्रकार और साहित्य संस्कृतिकर्मी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से झगडऩे जैसी स्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विचारधारा, सत्ता या प्रतिपक्ष से जुड़ाव तक मतभेद समझ में आ सकते हैं। लेकिन प्रतियोगिता अथवा निजी नाराजगी में एक दूसरे को अपराधीदेशद्रोही तक करार देने की पराकाष्ठा से या किसी को लाभ हो सकेगा? अभिव्यति की स्वतंत्रता तो संविधान में हर भारतीय नागरिक को है। समाचार माध्यमों-पत्र पत्रिकाओं टीवी चैनल भी उसी अधिकार का लाभ पाते हैं। फिर कुछ नियम प्रावधान मीडिया के लिए बनते बदलते रहे हैं। इसलिए इन दिनों मीडिया के कई दिग्गज, राजनेता, सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग और सामान्य जनता का एक वर्ग किसी लगाम, नियंत्रण, लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं। उन्हें ध्यान नहीं है, यह बात पिछले पांच दशकों में उठती और दबाई जाती रही है।
मैं स्वयं 1970 से पत्रकारिता में होने के कारण राज्यों और केंद्र की सरकारों, अतिवादी सांप्रदायिक, आतंकवादी समूहों के दबावों और प्रयासों को देखता, समझता और झेलता रहा हूं। वर्तमान सन्दर्भ में टीवी मीडिया को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है। वे यों सुशांत सिंह-रिया प्रकरण या चीन भारत सीमा विवाद या कोरोना महामारी के संकट को दिन रात अतिरंजित ढंग से दिखा रहे हैं। फिर प्रतियोगिता में एक दूसरे से मार काट यों कर रहे हैं? कौन कितना किस विषय को दिखाए यह तय कौन करेगा? वास्तव में एक गंभीर कोशिश का ध्यान आता है। बात 2006 की है। उस समय मैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया का अध्यक्ष था और साथी वरिष्ठ संपादक सच्चिदानन्द मूर्ति महासचिव पदों पर थे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस गठबंधन की सरकार सत्ता में थी। सरकार ने मीडिया के ब्रॉडकास्ट नियामक विधेयक तैयार कर लिया। इससे पहले केवल केबल प्रसारण के नियमन के लिए कुछ नियम कायदे बने हुए थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े नेता-मंत्री टीवी चैनलों की बढ़ती संया और उपभोता अधिकार के बहाने समूर्ण इलेट्रॉनिक मीडिया को कड़े कानून में बांधना चाहते थे। इस विधेयक में भारत के सभी सरकारी स्वायत्ता और निजी रेडियो टीवी चैनल के प्रसारण के विषय, लिखी बोली दिखाई जाने वाली सामग्री तक पर सरकार की निगरानी का प्रावधान था। मेरी और मुझसे वरिष्ठ संपादक बीजी वर्गीज, कुलदीप नायर, मामन मैथ्यू सहित पत्रकारों की नजर में यह प्रस्तावित कानून एक मायने में आपातकाल के सेंसरशिप से भी अधिक खतरनाक था।
इससे पहले प्रिंट माध्यम के लिए बिहार में लाया गया कानून या राजीव गांधी के सत्ता काल में आये प्रेस कानून का एडिटर्स गिल्ड तथा पत्रकार संगठनों और प्रतिपक्ष ने भी विरोध किया था। इसलिए मनमोहन सिंह की सरकार के प्रस्तावित विधेयक को क़ानूनी रूप मिलने से पहले हम सबने कड़ा विरोध अभियान शुरू कर दिया। गिल्ड के पदाधिकारी के नाते मंत्रियों, सूचना-प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार (पूर्व पत्रकार भी) आदि के साथ बैठकें हुई। इस कारण सरकार कुछ संशोधन इत्यादि पर विचार करने लगी। संयोग से तत्कालीन सूचनाप्रसारण मंत्री प्रिय रंजन दासमुंशी अस्वस्थ्य हो गए। इस कारण भी विधेयक रास्ते में अटक गया। फिर भी आशंका से चिंतित संपादकों ने वार्ताओं का सिलसिला जारी रखा।यहां यह बात भी उल्लेख करना उचित होगा कि पहले गिल्ड केवल उन संपादकों कि संस्था बनी थी, जो अखबार या पत्रिका में प्रकाशन के सम्पूर्ण संपादक हों। मीडिया का विस्तार होने पर हमने टीवी समाचार चैनल के प्रमुख संपादकों को भी सदस्य बनाया। सदस्यता के लिए भी वरिष्ठ संपादकों की चयन समिति रही, ताकि निर्धारित मानदंडों वाले ही सदस्य बने। इस नए संकट में हमने एडिटर्स गिल्ड की तरफ से यह सुझाव दिया कि समाचार चैनल के संपादकों का एक सहयोगी संगठन स्वयं अपनी आचार संहिता तय कर लेगा और इसके लिए किसी सेवानिवृत्ता वरिष्ठ न्यायाधीश को भी मार्गदर्शन के लिए रखा जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रमुख न्यायाधीश जेएस वर्मा जी को यह दायित्व सौंपा गया।
इस तरह महीनों के कड़े विरोध, बातचीत और प्रस्तावों से वह विधेयक सरकार ने ठंडे बस्ते में रख दिया। एडिटर्स गिल्ड में हरि जयसिंह के अध्यक्ष और मेरे महासचिव के कार्यकाल में संपादकों के लिए एक आचार संहिता बनाई गई और राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वयं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एक छोटे सभाकक्ष में आकर उसे जारी किया था। इसी तर्ज पर 2007 से टीवी संपादकों और खासकर प्रसारण के लिए अपने नियम आचार संहिता बनाई। मेरे जैसे कितने ही संपादक और पत्रकार, विधिवेत्ता, सांसद समय-समय पर संवैधानिक मान्यता प्राप्त भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य भी रहे हैं। पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश उसके अध्यक्ष रहते हैं। प्रेस परिषद् ने भी बहुत नियम आचार संहिता बनाई, लेकिन कानूनी रूप से उसका दायरा अब तक प्रिंट मीडिया तक सीमित रहा है। परिषद् या संपादकों की आचार संहिताओं में किसी सजा का प्रावधान नहीं है। मतलब इसे अपने जीवन मूल्यों की तरह स्वयं अपनाए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस पृष्ठभूमि में आज भी सवाल यह है कि प्रकाशन या प्रसारण की सामग्री और प्राथमिकता कौन तय करे? अपराध कथा को प्रथमिकता मिले या राजनीति या आर्थिक या मनोरंजक या व्यापारिक, फिल्मी, क्रिकेट या कबड्डी… हजारों विषय समाज में और दुनिया में हैं।
कौन कितनी देर या दिखाए या बोले- कौन तय करे। इन दिनों महाप्रगतिशील वर्ग तो पहले ही मीडिया को बिका हुआ, डरा हुआ कहकर बदनाम किए हुए हैं। अभी तो संसद में भी यह मुद्दा उठ सकता है। हम सब शुचिता के साथ स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचे दिखाकर भत्र्सना के साथ या क्रोध या रुदन के बाद सरकार को प्रसारण नियामक कानून बनवाने के लिए निमंत्रित करना चाहेंगे? सरकार किसी भी पार्टी की हो, प्रतिपक्ष का एक खेमा तो प्रसन्न ही होगा। सत्ता तो आती जाती रहती है। कानून तो हमेशा रहेगा। वैसे भी भारत के पुराने प्रेस कानून में संशोधन के एक प्रस्ताव पर विचार विमर्श जारी है। प्रसारण और सोशल मीडिया पर आवाज उठने से सरकार को कहां कोई नुकसान होगा। हां, अभिव्यति की स्वतंत्रता की आवाज उठाने वाले ही घायल होंगे और सामान्य नागरिक भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा बनाई जा सकने वाली नियामक व्यवस्था से चुनी गई सामग्री ग्रहण कर सकेंगे। आपसी लड़ाई के दौरान सबको भविष्य को ध्यान में रखकर स्वयं तय करना होगा। आत्म अनुशासन या सरकारी लगाम?
आलोक मेहता
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं ये उनके निजी विचार हैं)