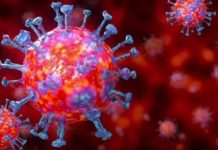उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल परशुराम की चर्चा गर्म है। केएम मुंशी ने अपनी रचना ‘भगवान परशुराम’ में उन्हें कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के दमनकारी राज्य के खिलाफ गिरिजनों और वनवासियों को संगठित करते हुए दिखाया है। परशुराम ने अघोरियों के गुरु से अघोर विद्याएं सीखीं और सत्ता के खिलाफ युद्ध में जनबल के साथ उनका भी निर्णायक इस्तेमाल किया। यहां परशुराम का किरदार ब्राह्मणवादी, कर्मकांडी, पुरोहित या वेदपाठी नहीं है। उनकी राजनीति सत्ताधारियों को चुनौती देने की है। प्रश्न यह है कि पिछड़ी और दलित जातियों की राजनीति करने वाली यूपी की पार्टियां (सपा और बसपा) या ऐसे परशुराम और उनके राजनीतिक फरसे का सत्ता विरोधी इस्तेमाल कर पाएंगी? क्या, क्या भाजपा के पाले से ब्राह्मणों को खींच लेने की जुगाड़ में लगी कांग्रेस इसके जरिये अपने पुराने वोट बैंक के एक हिस्से को फिर से प्राप्त कर पाएगी? कांग्रेस, सपा और बसपा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भाजपा परशुराम की किंवदंती के राजनीतिक प्रभाव से कुछ चिंतित है।
उनकी दलील है कि अगर ऐसा न होता तो योगी सरकार 2017 में अपनी तीसरी कैबिनेट बैठक में ही परशुराम जयंती की छुट्टी खत्म न करती (इसके साथ महाराणा प्रताप और अग्रसेन जयंती की छुट्टियां भी खत्म की गई थीं)। जो भी हो, ये पार्टियां योगी बनने से पहले मुख्यमंत्री की जाति और मीडिया- चर्चाओं पर आधारित उनकी सरकार के कथित राजपूत रुझान के साथ परशुराम के क्षत्रिय-विरोध को जोड़कर ब्राह्मण- असंतोष को भुनाना चाहती हैं। एक माह पूर्व विकास दुबे एनकाउंटर और उससे कुछ पहले उसी जाति के दो एनकाउंटरों के आधार पर ये पार्टियां दिखाना चाहती हैं कि योगी की सरकार ब्राह्मण-बाहुबलियों के पीछे पड़ी हुई है।इन पार्टियों ने वादा किया है कि वे परशुराम की ऊंची से ऊंची मूर्ति भी स्थापित करेंगी। यूपी के ब्राह्मण मतदाता पिछले तीस साल से भाजपा को (वह चुनाव में जीते या हारे) निष्ठापूर्वक वोट दे रहे हैं। इस प्रदेश की आबादी में उनकी संया करीब ग्यारह फीसदी है, और इस लिहाज़ से वे एक बेहद प्रभावी वोटिंग समुदाय बनाते हैं।
इस दौरान भाजपा ने कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, मायावती और योगी आदित्य नाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। इनमें से कोई ब्राह्मण नहीं है। जाहिर है कि यूपी के ब्राह्मण अपनी जाति के व्यति को मुख्यमंत्री बना देखने के लिए भाजपा को वोट नहीं देते। इससे पहले वे जब कांग्रेस को वोट देते थे, उस समय भी कई बार गैरब्राह्मणों को मुख्यमंत्री पद मिलने के बावजूद उन्होंने उस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। वैसे भी यूपी के ब्राह्मण मतदाताओं की परंपरा क्षेत्रीय दलों का साथ ना देकर राष्ट्रीय पार्टियों का ही साथ देने की है। 2007 में बसपा की जीत में ब्राह्मण वोटों का योगदान 15 फीसदी से कम ही था। या यह एक विडंबना नहीं है कि मुय तौर पर कमजोर जातियों की गोलबंदी पर टिकी होने के बावजूद बसपा और सपा ब्राह्मण वोटों की फिराक में हैं, जबकि यादव और जाटव समुदायों को छोड़कर बाकी छोटी-छोटी कमजोर जातियां इन दलों का साथ छोड़कर पिछले तीन चुनावों में भाजपा की तरफ झुक चुकी हैं?
अगर ये पार्टियां अपने इस स्वाभाविक समर्थन आधार को वापस जीतने की रणनीति बना सकती हैं, तो शायद परशुराम का प्रतीक उनकी मदद कुछ ज्यादा कर सकेगा।अगर यह मान भी लिया जाये कि ब्राह्मण वोटर योगी सरकार से असंतुष्ट हैं, तो भी वे उस समय तक भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें इस पार्टी के साथ पचास फीसदी से ज्यादा का समर्थन आधार दिखता रहेगा। दूसरे, ब्राह्मण वोट अतीत की कांग्रेस की भांति अब भाजपा को अपनी स्वाभाविक पार्टी मानते हैं। मुख्यमंत्री किसी भी जाति का हो, वे जानते हैं कि भाजपा में उनके लिए कुछ न कुछ रहेगा। सपा-बसपा का वर्तमान और अतीत दोनों ही ब्राह्मण वोटों को इस तरह का कोई आश्वासन नहीं देता।
अभय कुमार दुबे
( लेखक सीएसडीएस, दिल्ली में प्रोफेसर और भारतीय भाषा कार्यक्रम के निदेशक हैं ये उनके निजी विचार हैं)