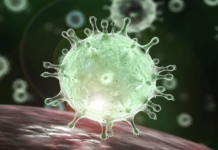स्वतंत्र भारत में नौकरशाही को सामंती सोच से अलग करके सेवाव्रती बनाने के लिए अनुच्छेद 310 के तहत उसे जो संरक्षण दिया गया, उस पर संविधान सभा में जोरदार बहस हुई थी। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि भविष्य में इसका फायदा उठाकर नौकरशाही जनरुचि के कामों में बाधाएं खड़ी करने लगेगी। कुछ तपे-तपाए सदस्यों को इस व्यवस्था से लोकशाही की अवधारणा के ही खतरे में आने का डर था। तब सरदार पटेल ने इस संवैधानिक संरक्षण का बचाव करते हुए कहा था कि आने वाले responsibleदिनों में इस बात की गारंटी नहीं है कि राजनीतिक अगुआ स्वाधीनता सेनानियों की तरह त्यागी और तपस्वी ही होंगे। हो सकता है कि भविष्य में अपने निजी उद्देश्यों के लिए वे नौकरशाही को दबाव में लेने की कोशिश करें। ऐसा हुआ तो यह व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। इसलिए सिस्टम चलाने वालों के लिए संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
सच हुईं आशंकाएं संविधान लागू हुए सत्तर साल हो गए हैं। इस बीच नौकरशाही का जो स्वरूप उभरा है, अपवादों को छोड़ दें तो उससे संविधान सभा के सदस्यों की आशंकाएं ही सही साबित होती नजर आ रही हैं। देश में कदाचार और भ्रष्टाचार की कहानियां सत्तर के दशक से बढ़नी शुरू हुईं। राजनीति पर पैनी निगाह रखने वाले कुछ जानकारों का मानना है कि नेताओं को भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करने में सरकारी तंत्र के प्रभावी वर्ग की बड़ी भूमिका रही। जिन लोगों का भी पाला सरकारी तंत्र से पड़ा है, वे मानते हैं कि नौकरशाही ने व्यवस्था को सहजता की ओर मोड़ने की बजाय उसे और जटिल ही बनाया है। अमूमन सत्ता के शीर्ष केंद्र की तरफ से खुले तौर पर कभी इस व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया जाता। माना जाता है कि इससे नौकरशाही नाराज हो सकती है।
हालांकि 2002 में बाल श्रम पर आयोजित देशभर के जिलाधिकारियों की कार्यशाला के समापन समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि अगर अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो इस कार्यशाला की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि प्रशासनिक सुधार के लिए कोशिशें नहीं हुईं। 1966 में मोरारजी देसाई और 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इन कमियों पर विचार करने और नौकरशाही में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए गए। लेकिन इनकी रिपोर्टों पर अमल नहीं हो पाया। माना जा सकता है कि नौकरशाहों के दबाव में ही राजनीतिक तंत्र यह काम नहीं कर पाया।
मोदी सरकार द्वारा ‘मिशन कर्मयोगी’ की घोषणा उसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार के मुताबिक इस मिशन का उद्देश्य है, सिविल सेवा अधिकारियों को क्रिएटिव, इनोवेटिव, प्रो-एक्टिव और तकनीकी तौर पर दक्ष बनाकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। लोकतांत्रिक देश में नौकरशाही को नवाचारी और लोकोन्मुखी ही होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थितियां अपवाद स्वरूप ही दिखती हैं। आज सरकारी तंत्र जिस मानसिकता से ग्रस्त है, उसमें बदलाव लाना बेहद चुनौतीपूर्ण है।
आजादी के बाद माना गया था कि नौकरशाही वैसी नहीं रहेगी, जैसी अंग्रेजों की थी। नौकरशाही को चुनने के लिए लोक सेवा आयोग की अवधारणा का मतलब भी यही था कि चुने गए लोग लोक के सेवक होंगे। हकीकत में देखें तो भारतीय नौकरशाही ‘यस मिनिस्टर’ का विस्तारित रूप बनती चली गई। आजादी के आंदोलनों से क्रूरतापूर्वक निबटने वाली अंग्रेज नौकरशाही का सामना कर चुकी पीढ़ी अब अपने अवसान की ओर है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के प्रति उसका क्षोभ कई बार इतना बढ़ जाता है कि उसके लोग भी यहां तक कह देते हैं कि अंग्रेजी व्यवस्था आज से कहीं बेहतर थी। मौजूदा सरकारी तंत्र में कर्मठ और लोकोन्मुखी लोग भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। जिस तरह की व्यवस्था विकसित हो गई है, उसमें ढलना या चुप पड़े रहना एक दौर के बाद उनकी मजबूरी बन जाती है।
एक पूर्व अधिकारी नौकरशाही की मानसिकता को विश्लेषित करते हुए कहते हैं, ‘जब भी किसी जिम्मेदार अधिकारी के सामने कोई प्रस्ताव आता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उसे टालने की होती है। अगर वह टाल नहीं पाता तो प्रस्ताव में वह पहले अपना फायदा देखता है। जरूरी नहीं कि वह आर्थिक ही हो।’ उनके मुताबिक, ‘प्रस्ताव पर फैसला लेते वक्त अधिकारी सोचता है कि इससे उसकी अगली पोस्टिंग या प्रमोशन में कोई फायदा मिल सकता है या नहीं। अगर ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती तो वह अपने बैच का लाभ देखने की कोशिश करता है। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो वह अपने संवर्ग के बारे में सोचता है। संवर्ग यानी अगर वह आईएएस है तो आईएएस के बारे में सोचेगा, आईपीएस है तो आईपीएस या आईआरएस है तो आईआरएस के बारे में।’
ऐसे मानस में लोक कहां रह जाता है? पूर्व अधिकारी का मानना है कि कहीं न कहीं, अधिकारियों के प्रशिक्षण में ही कमी है। इसी वजह से उनमें लोकोन्मुखी होने का भाव नहीं भर पाता और यही वजह है कि देश में अब तक जैसा जमीनी बदलाव दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है। भारतीय नौकरशाही के बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि वह भावी चुनौतियों को देख पाने की क्षमता विकसित करने में सफल नहीं हो पाई है।
सवालों से परे जब कोई बांध टूटता है, कोई पुल गिरता है या नगरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, तब राजनीति जरूर सवालों के घेरे में आती है लेकिन जर्मन राजनीतिशास्त्री मैक्स वेबर के शब्दों में कहें तो सरकारी तंत्र के स्टील फ्रेम पर सवाल कम उठते हैं। संविधान प्रदत्त संरक्षण उसे ज्यादातर मामलों में बचा ले जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीति और राजनेता हमेशा लोक के रडार पर रहते हैं। सत्ता में चाहे जो भी दल हो, उसकी मीनमेख निकाली ही जाती है। मीडिया और आज के सोशल मीडिया के निशाने पर भी जितनी राजनीति रहती है, उतनी नौकरशाही नहीं। उम्मीद की जानी चाहिए कि मिशन कर्मयोगी तंत्र को मानस के स्तर पर भी भारतीय बनाने में कामयाब हो सकेगा।
उमेश चतुर्वेदी
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके निजी विचार हैं)