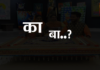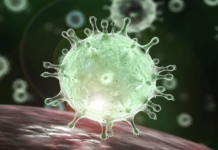कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है नींद क्यों रात भर नहीं आती! हां, मिर्जा गालिब का यह शेर देश की कम्युनिस्ट पार्टियों की मौजूदा हालत पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कहीं से, किसी भी कोने से साम्यवादी राजनीति के लिए उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। बावजूद इसके उसके पुनर्जीवित होने की बेचैनी भी खत्म नहीं हो रही है! एक तरफ लोग उनका मृत्यु लेख लिखने को आतुर हैं तो दूसरी ओर देश के हालात ऐसे बन रहे हैं, जो लेफ्ट की राजनीति के फलने फूलने के बिल्कुल मुफीद हैं।
तस्वीर क्या ही अजब! एक तरफ पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चा जड़ से उखड़ चुका है। देश की दूसरी सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म होने वाला है। सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम भी चुनावी राजनीति के लिहाज से अप्रासंगिक है। केरल में जरूर उसका गढ़ बचा हुआ है पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वहां भी उसकी जड़ हिला दी। साम्यवाद के उस किले का ढहना भी महज वक्त की बात है। संसद में उसका प्रतिनिधित्व सिकुड़ते-सिकुड़ते ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां उसके होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। पर दूसरी ओर देश में बढ़ती आर्थिक असमानता, रोजगार के संकट, उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था पर मंडराते संकट और बढ़ते सामाजिक तनाव से उनकी वापसी की जमीन और संभावना भी बनती है।
सवाल है क्या इस स्थिति से उबरने, फिर से अपने पैरों पर खड़े होने और अपने हारे हुए गढ़ में वापस जीत हासिल करने का माद्दा वामपंथी पार्टियों में है या भाजपा के इस प्रचार को मान लिया जाए कि साम्यवाद एक विदेशी विचारधारा है, जिसके लिए अब हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं बची? जब इसके लिए उन देशों में जगह नहीं बची, जहां इसका जन्म हुआ था तो भारत में यह आयातित विचारधारा कितने समय तक बची रह सकती है? जिस तरह से पूरी दुनिया में पूंजीवाद पर आधारित राष्ट्रवाद की आधुनिक विचारधारा का विस्तार हो रहा है और साम्यवादी व समाजवादी राजनीति की भौगोलिक व वैचारिक उपस्थिति सिकुड़ रही है वहीं प्रक्रिया अंततः भारत में भी दोहराई जानी है।
पर क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचाई यह नहीं है कि राजनीति में भले पूंजीवाद की वैकल्पिक विचारधारा का स्पेस सिकुड़ा है पर कम से कम आर्थिकी में उसके लिए स्पेस बचा हुआ है? और अगर वहां जगह बची हुई है तो फिर राजनीति में भी उस विचारधारा की वापसी के रास्ते बंद नहीं समझे जा सकते हैं। असल में मुक्त पूंजीवाद पर आधारित जिस आर्थिक व्यवस्था का जय जयकार हम पिछले तीन दशक से कर रहे थे उसका स्याह पक्ष खुल कर सामने आ गया है। उन्मुक्त पूंजी के लिए सारे रास्ते खोल देने की वकालत करने वालों को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गलती कहां हुई। वे अब बढ़ती आर्थिक असमानता से चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था और मुक्त पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था ने जिस समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता का वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ है।
कम्युनिस्ट पार्टियां अगर देश, समाज, राजनीति और आर्थिकी की इस हकीकत को समझती हैं और खुद को रिइन्वेंट करने का प्रयास करती हैं तो उनकी वापसी का रास्ता फिर से खुल सकता है। इसकी शुरुआत सभी वामपंथी पार्टियों के फिर से एकजुट होने से हो सकती है। साठ के दशक में विभाजन के बाद ये पार्टियां कहां पहुंचीं हैं, अगर वे उसका ईमानदार आकलन करें तो उनकी वापसी का रास्ता खुल सकता है। इस मामले में देश की साम्यवादी पार्टियां, समाजवादी पार्टियों से अलग हैं।
ऐसे समय में देश की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की कमान डी राजा को मिलना भी एक संयोग है। डी राजा को पिछले दिनों सीपीआई का महासचिव बनाया गया। देश में चल रहे दलित विमर्श के बीच एक दलित नेता का सीपीआई का महासचिव बनना इस लिहाज से बहुत खास है कि वे एक-एक सीढ़ी चढ़ कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। देश की राजनीति में उनकी एक स्वीकार्यता बनी है, जिसका इस्तेमाल वे कम्युनिस्ट एकता के लिए कर सकते हैं। धीरे धीरे जमीनी संघर्षों और सामाजिक सचाइयों से दूर होती गई कम्युनिस्ट पार्टियों को वे वापस उनके रास्ते पर लाने का प्रयास भी कर सकते हैं।
सीपीआई महासचिव डी राजा और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी दोनों खुले विचार के लोग हैं। समाज की बदलती सचाई को समझते हैं और राजनीतिक यथार्थ से भी परिचित हैं। इसलिए इन दोनों के ऊपर व्यावहारिक समाधान निकालने की जिम्मेदारी है। इन्हें समझना होगा कि कांग्रेस से तालमेल करने या विपक्षी पार्टियों की एकजुटता बनाने की राजनीति से पहले लेफ्ट को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसके लिए मौजूदा वक्त से बेहतर समय नहीं हो सकता है।
अजित द्विवेदी
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके निजी विचार हैं…