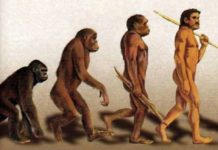भारत सरकार और किसान संगठनों के बीच अभी तक जो बातचीत हुई है वह एक किस्म की औपचारिकता है, जिसे दोनों निभा रहे हैं। हर आंदोलन में ऐसा होता है। सुलह-सफाई की शुरुआत ऐसी ही औपचारिक बातचीत से होती है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद ठोस प्रस्तावों पर बात करनी होती है। उसका समय अब आ गया है। पांच बार वार्ता करके किसान उब गए हैं। तभी उन्होंने पांचवें दौर की वार्ता के समय मौन व्रत धारण कर लिया था। वे सरकार से अब अपने सवालों का जवाब सुनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार दो टूक जवाब दे। इस दो टूक जवाब के लिए ही किसान संगठनों ने आंदोलन की तीव्रता भी बढ़ा दी है। आठ दिसंबर का भारत बंद इस मामले में निर्णायक हो सकता है। भारत बंद को देश के तमाम मजदूर संगठनों और कई पार्टियों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। नौ दिसंबर को होने वाली वार्ता से पहले अगर किसानों का भारत बंद सफल होता है तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बढ़ेगा।
अब सवाल है कि इस दबाव में या ओवरऑल किसान आंदोलन के दबाव में सरकार किसानों को क्या दे सकती है? अगर इस पहलू से विचार करें कि सरकार के पास क्या विकल्प हैं तो बहुत ज्यादा विकल्प दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार भी घूम फिर कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था को जारी रखने की गारंटी देने पर लौट आ रही है। बाकी जो चीजें सरकार की ओर से किसानों को ऑफर की जा रही हैं वो बहुत छोटी और तकनीकी चीजें हैं, जो इतनी अहम नहीं हैं कि उन पर वार्ता बन या बिगड़ जाए। सो, अभी तक सरकार की ओर से किसानों को जो मिलता दिख रहा है वह एमएसपी की गारंटी है। हालांकि उस गारंटी का भी स्वरूप स्पष्ट नहीं है। ध्यान रहे गिने-चुने फसलों पर ही एमएसपी की व्यवस्था लागू है।
सो, सरकार की मंशा एमएसपी की गारंटी का वादा किसान को थमा कर आंदोलन खत्म कराने की है। दूसरी ओर किसान की तैयारी तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने तक आंदोलन करने की है। इन दोनों के बीच में क्या रास्ता हो सकता है? कायदे से बीच का कोई रास्ता नहीं बनता है। सरकार को खुले दिल से यह स्वीकार करना चाहिए कि कम से कम देश के किसान और कृषि क्षेत्र का भला करने के लिए इन तीनों कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का कोई अलग एजेंडा हो, खेती-किसानी की बजाय कृषि कारोबार से जुड़े बड़े उद्यमियों को फायदा पहुंचाना हो, खाद्य सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निजी सेक्टर पर डालने की सोच हो और कारपोरेट फार्मिंग को स्थापित करना मकसद हो तो अलग बात है, अन्यथा इन तीनों कानूनों से देश के किसानों और कृषि सेक्टर का तो कोई भला नहीं होने वाला है।

अपने बनाए कानूनों की तारीफ करते हुए सरकार जो बार बार कह रही है ‘वन नेशन, वन मार्केट’ बना दिया गया है, आखिर उसकी जरूरत किसको है? क्या इस कानून से पहले देश के एक राज्य के किसान का सामान दूसरे राज्य में नहीं बिकता था? क्या कश्मीर और हिमाचल के सेब देश भर में नहीं जाते थे? महाराष्ट्र का संतरा और प्याज देश भर में नहीं बिकता था? कर्नाटक के अंगूर या बिहार का चावल क्या देश के दूसरे हिस्सों में नहीं बिकता था? मंडियों की व्यवस्था के तहत पहले से ही पूरा देश एक बाजार था। इसे जबरदस्ती एक जुमला बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरे, अगर कृषि कानून इतने ही अच्छे हैं तो देश भर के किसान उनके समर्थन में उतरते क्यों नहीं हैं? कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ छह फीसदी खरीद एमएसपी पर होती है, देश के बाकी किसानों को आंदोलन से मतलब नहीं है तो फिर बाकी किसान आंदोलन के विरोध में क्यों नहीं उतर रहे हैं? बाकी किसान ‘वन नेशन, वन मार्केट’ के समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में बहुत गर्व से कहा कि बिहार में जो व्यवस्था 2006 में लागू की गई थी उसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है तो सवाल है कि बिहार के किसान खुल कर इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? चाहे बिहार का किसान हो या मध्य प्रदेश का, वह भी क्यों किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है? अगर आंदोलन सिर्फ छह फीसदी किसानों का है और बाकी 94 फीसदी को सरकार के कानून से फायदा होना है तो अब तक देश में कानून के समर्थन में 94 फीसदी किसानों का आंदोलन शुरू हो जाना चाहिए था?
दूसरी दिलचस्प बात यह है कि देश के जितने भी गुरचरण दास, हरचरण दास किस्म के कारपोरेट अर्थशास्त्री हैं, वे सब सरकार के बनाए कानूनों के समर्थन में उतरे हुए हैं। किसान और कृषि के विशेषज्ञ इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कारपोरेट अर्थशास्त्री आंदोलन का विरोध और कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। इससे भी यह साफ होता है कि इन कानूनों का किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार की मंशा पर सवाल इन कानूनों की टाइमिंग के कारण भी उठ रहा है। इस समय सारी दुनिया में विकसित देश अपने यहां खेती-किसानी को संरक्षण देकर, सब्सिडी देकर बचाने की नीति पर चल रहे हैं और ऐसे समय में भारत में सुधारों की सोची गई! यह सुधार का समय नहीं है, बल्कि किसान और खेती दोनों को बचाने का समय है। इसके लिए सरकार, जो किसानों को दे सकती है वह न्यूनतम आय की गारंटी है। जैसा अमेरिका, यूरोप आदि में किया जा रहा है। अमेरिका में इस साल किसानों को 46 अरब डॉलर की सब्सिडी दी जा रही है। यह अमेरिका के कुल खाद्यान्न उत्पादन की 40 फीसदी कीमत के बराबर है। यूरोपीय देशों में हर साल 54 अरब यूरो की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में यह कहां की समझदारी है कि कृषि सुधार के नाम पर भारत के किसानों की किस्मत कारपोरेट के हवाले कर दी जाए?
नया बाजार मिलेगा, नया खरीदार मिलेगा, नई तकनीक मिलेगी, यह सब कह कर किसानों को बरगलाने की बजाय सरकार को चाहिए कि वह समग्रता से तीनों कानूनों पर विचार की हामी भरे। अभी समय भी है, सरकार चाहे तो संसद का एक छोटा सत्र बुला सकती है। पिछले सत्र में जैसे सरकार ने जोर जबरदस्ती कृषि विधेयकों को पास कराया था, उस गलती को इस सत्र में सुधारा जा सकता है। किसानों और विपक्ष की राय से सरकार इन कानूनों को बदल सकती है। अगर देश का किसान ठेके पर खेती के लिए नहीं तैयार है तो उसे इसके लिए मजबूर करने की बजाय उसकी इच्छा को सर आंखों पर रखना चाहिए। अगर उसे अपना अनाज मंडियों में बेचना है और सरकार की तय की गई कीमत पर ही बेचना है तो इस इच्छा का भी सम्मान करना चाहिए। यह कोई ऐसी चीज नहीं है, जो सरकार किसानों को नहीं दे सकती है।
अजीत द्विवेदी
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं ये उनके निजी विचार हैं)