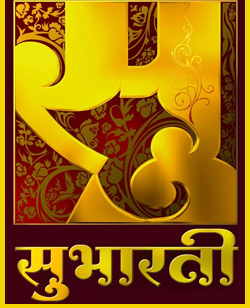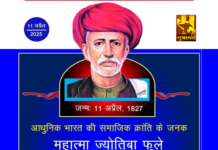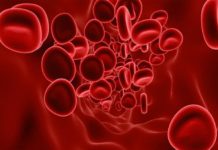कई बार यह जरूरी होता है, खास कर युद्ध के समय या प्राकृतिक-कृत्रिम आपदा के समय या चिकित्सा महामारी के समय कि समूचा देश उस जुबान में बात करे, जो सरकार की जुबान होती है। सरकार को जो सही लगे वह उसे करने दिया जाए। उसके फैसलों पर सवाल नहीं उठाया जाए और न उसके अमल में अड़ंगा लगाया जाए। परंतु असहमति को लोकतंत्र की बुनियाद मानने वाले कई लोग इसे सही नहीं मानते हैं। जैसे पिछले दिनों मशहूर वकील दुष्यंत दवे ने लिखा कि यह कैसा समय है, जब विधायिका और न्यायपालिका दोनों का काम लगता है स्थगित हो गया है और सिर्फ कार्यपालिका ही देश चला रही है। इसके जवाब में एक दूसरे मशहूर वकील हरीश साल्वे ने लिखा कि इस समय अदालतों को किसी हाल में कार्यपालिका को फैसले करने से नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे फ्रांस में चुनाव स्थगित हो गए या कैसे ब्रिटेन में कार्यपालिका को असीमित अधिकार मिला है या अमेरिका में इस समय जैसी पाबंदियां लगी हैं, सामान्य स्थितियों में उसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक माना जाएगा।
भारत में हरीश साल्वे को यह कहने की जरूरत नहीं है। यहां वैसे भी कार्यपालिका ही काम कर रही है और लोकतंत्र का कोई दूसरा स्तंभ न तो उस पर सवाल उठा रहा है और न उसके रास्ते में अड़ंगा बन रहा है। वैसे भी भारत में विधायिका का कोई खास मतलब नहीं होता है। असली मतलब सरकार का होता है। कायदे से विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है और उसका दर्जा ऊपर होना चाहिए पर भारत में विधायका हमेशा कार्यपालिका के पीछे चलने वाली और उसकी हर बात में हामी भरने वाली संस्था ही रही है। सत्तारूढ़ दल, सरकार या प्रधानमंत्री जो भी फैसला करता है उस पर आमतौर पर विधायिका की मुहर लगती है। अगर सरकार अपने दम पर बहुमत में हो, जैसे अभी है तो बिना अपवाद के सरकार के हर फैसले पर विधायिका की मुहर लगती है। इसलिए विधायिका की भूमिका पर विचार करना बेकार है।
कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण रखने और उसे राह दिखाने के लिए दो और संस्थाओं- न्यायपालिका और प्रेस को लोकतंत्र का स्तंभ माना गया। पर ऐसा लगता है कि इन दोनों संस्थाओं ने भी ‘जो तुमको हो पसंद, वहीं बात कहेंगे’ को अपना मूल सिद्धांत बना लिया है। जैसे ही मीडिया में कोई बात जोर-शोर से चलना शुरू होती है वैसे ही लोग समझ जाते हैं कि यह सरकार का एजेंडा है और जैसे ही कोई मामला न्यायपालिका के सामने पहुंचता है वैसे ही अंदाजा लग जाता है कि इसमें फैसला वहीं आएगा, जो सरकार चाहती है। हो सकता है कि यह महज संयोग हो, पर आमतौर पर ऐसा ही होता है।
जैसे सिर्फ कोरोना के समय की ही बात करें तो एक के बाद एक कई फैसले आए हैं, जो सरकार की सोच और उसके फैसले के बिल्कुल संगति में थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, जिसकी खूब वाहवाही भी हुई पर दो-चार दिन के बाद ही उसे फैसला बदलना पड़ा। अदालत ने आदेश दिया था कि हर व्यक्ति की कोरोना वायरस से संक्रमण की जांच बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। सर्वोच्च अदालत के आदेश में यह भी कहा गया था कि निजी या सरकारी लैब कोई भी हो जांच मुफ्त में होनी चाहिए और सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए कि निजी लैब्स को उनके खर्च का पैसा मिल जाए।
सरकार को यह फैसला पसंद नहीं आया और इसलिए उसने इस बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की। निजी लैब्स के खर्च की भरपाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से निजी लैब्स वाले अदालत पहुंच गए और अदालत ने सरकार की भावना को समझते हुए अपना आदेश संशोधित कर दिया। उसने कहा कि सिर्फ उन्हीं लोगों की जांच मुफ्त में होगी, जो आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर होते हैं यानी गरीब हैं। इसके कुछ दिन के बाद खबर आई कि भारत सरकार का अब तक जांच पर हुआ कुल खर्च एक सौ करोड़ रुपए है। सोचें, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सबसे बड़ी महामारी की जांच पर एक सौ करोड़ का खर्च है और उधर 33 करोड़ वाले अमेरिका ने अपने यहां सिर्फ जांच के लिए साढ़े सात हजार करोड़ रुपए जारी किए हैं ताकि हर व्यक्ति की मुफ्त जांच हो सके!
ऐसे ही विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने का आदेश देने के लिए एक याचिका अदालत में दायर की गई। सरकार ने कहा कि वह अभी लोगों को नहीं निकाल सकती है तो अदालत ने आदेश दिया कि जो जहां है अभी वहीं रहे। प्रधानमंत्री के बनाए पीएम-केयर्स फंड की वैधता को लेकर याचिका दायर की गई तो अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया। यहां तक कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सबसे अधिक संभावना वाले समूह के लोगों यानी नर्सों और स्वास्थकर्मियों ने अदालत में याचिका दी कि उनकी सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करने के आदेश दिए जाएं तो अदालत ने वह याचिका भी खारिज कर दी क्योंकि सरकार ने कहा कि वह उपाय कर रही है। वैसे तो कई मामलों में अदालतें मीडिया को निर्देश देती रही हैं, जैसे जय शाह का मामला मीडिया में न छपे या बाबा रामदेव के बारे में लिखी गई किताब न छपे और उसके अंश भी मीडिया में न आएं, अभिषेक मनु सिंघवी के पिता के बारे में लिखी गई किताब प्रकाशित न हो आदि पर मीडिया में कोरोना वायरस को कम्युनल तरीके से पेश करने, उसे हिंदू-मुस्लिम का रंग देने वाली खबरों पर रोक के लिए जब जमात ए उलेमा ए हिंद ने अदालत में याचिका दी तो उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि अदालत मीडिया पर रोक नहीं लगा सकती।
सोचें, ऐसा तालमेल निकट अतीत में कब देखने को मिला था? कोई ताजा स्मृति नहीं है। मिसाल ढूंढने के लिए पिछली सदी के सातवें दशक में ही जाना होगा। हालांकि मीडिया ने तब भी हिम्मत दिखाई थी। पर आज का दौर जरा अलग है।
अजीत दि्वेदी
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं ये उनके निजी विचार हैं)