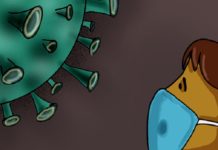बीते दिनों ओलिंपिक और पैरालिंपिक खिलाड़ियों की सफलताएं चर्चा में रहीं। उनके सम्मान में कई आयोजन हुए। लेकिन क्या तस्वीर खिंचवाने के अवसर और सुनियोजित कार्यक्रम सिर्फ देखने के लिए हैं या आखिरकार अब भारत को मजबूत ओलिंपिक राष्ट्र के रूप में देखा जा सकता है? प्रधानमंत्री और खेल मंत्रालय वैध रूप से दावा कर सकते हैं कि उन्होंने ओलिंपिक पदक की तैयारी में पिछली सरकारों की तुलना में ज्यादा काम किया है।
खेल मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू की गई टार्गेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) योजना की ओलिंपिक और पैरालिंपिक खिलाड़ियों को पहचानने और मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खासतौर पर पहले ओलिंपिक सिल्वर मेडलिस्ट राज्यवर्धन राठौर और फिर युवा किरेन रिजिजू द्वारा खेल मंत्रालय संभालने के बाद मिशन टोक्यो की तैयारी में स्पष्ट बदलाव दिखा। विभिन्न निजी ट्रस्ट और फाउंडेशन ने भी ऐसा ईको-सिस्टम बनाने में मदद की जहां खिलाड़ी वास्तव में गोल्ड जीतने की महत्वाकांक्षा रख पाएं।
इससे विपरीत पिछली यूपीए सरकार में खेल मंत्रालय हाशिये पर था और उसे कई मंत्रियों के बीच घुमाया जाता रहा। यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच 6 खेल मंत्री रहे। उनके मणिशंकर अय्यर जैसे खेल मंत्री भी रहे, जो खुलकर एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों के लिए बोली लगाने के प्रयासों से चिढ़ते थे। वहीं सुनील दत्त इसे ‘जूनियर’ पद मानकर नाखुश रहते थे। इसलिए मोदी सरकार को श्रेय जाता है कि उसने मंत्रालय को ज्यादा उत्साहजनक ‘खेलो इंडिया’ वाली पहचान देने की कोशिश की।
इन ओलिंपिक खेलों में इसके स्पष्ट संकेत मिले कि भारतीय प्रतिभागियों में अब प्रतिस्पर्धा की भावना है। वहीं पैरालिंपिक में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। इसलिए जश्न मनाना उचित लगता है। ऐसी पीढ़ी के लिए, जो हॉकी में मेडल जीतने की सीमित महत्वाकांक्षा के साथ बड़ी हुई, उसके लिए टोक्यो 2020 महत्वपूर्ण रहा है। एक ‘नए’ युवा भारत के लिए अब नीरज चोपड़ा जैसी प्रेरक शख्सियत हैं, जिससे उसकी महत्वाकांक्षा को पंख लग सकते हैं।
फिर भी इस उत्साह के बीच कुछ जमीनी हकीकतें भी याद रखनी होंगी। पदक विजेता भले ही मिले हों लेकिन देश में एथलीट के प्रदर्शन और ओलिंपिक खेल के समग्र स्तर के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। देश में कितने स्कूलों में खेल के मैदान और शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं जो युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं? जीतने वाले खिलाड़ियों को अच्छी फंडिंग से ही प्रतिस्पर्धी खेलों की संस्कृति विकसित नहीं होगी। इसके लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी की जरूरत है, जिससे खेलों का ऐसा माहौल बने जो इसे सिर्फ ओलिंपिक जैसे आयोजनों के ग्लैमर से न जोड़े।
ओडिशा सरकार की हॉकी में भागीदारी इसका अच्छा उदाहरण है कि एक प्रगतिशील राजनीतिक नेतृत्व जब तुरंत इनाम पाने की इच्छा के बिना एक ओलिंपिक खेल को अपनाता है तो नजीते कितने अच्छे हो सकते हैं। ओडिशा ने हॉकी का साथ तब दिया, जब देश के सभी सक्षम प्रायोजकों ने हार मान ली।
दिव्यांग खिलाड़ियों का संघर्ष भी देखना चाहिए। जब बात समावेशन और सुविधाओं की उपलब्धता की होती है तो दिव्यांगों को अब भी संघर्ष करना पड़ता है। देश में ऐसे कितने खेल केंद्र हैं जहां दिव्यांगों को आसान पहुंच देकर बराबरी का अवसर दिया जाता है? और कितने संस्थान हैं जो दिव्यांग लोगों को योग्य नागरिक मानते हैं और परोपकार करने के लिए ‘बेचारा’ नहीं? भारत में दिव्यांगों की वर्कफोर्स में भागीदारी अभी भी वैश्विक औसत से कम है और अधिकार कानून के बावजूद दिव्यांगों को न्याय पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है।
भविष्य की चुनौती में सबसे मुख्य है खेलों के लिए एकतरफा शासन संरचना। दशकों से, ज्यादातर खेल संघ राजनेताओं और उनके सहयोगियों की व्यक्तिगत जागीर की तरह चलाए जाते रहे हैं। अब जब निजी ट्रस्टों ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए कमी पूरी करने की कोशिश की है, तो यह विश्वास जागा है कि हमारे खेलों में नेता-बाबू संस्कृति खत्म होगी। लेकिन जब तक शासन का स्तर नहीं बढ़ता, खेल संघों को शक की निगाह से देखा जाता रहेगा।
राजदीप सरदेसाई
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं ये उनके निजी विचार हैं)