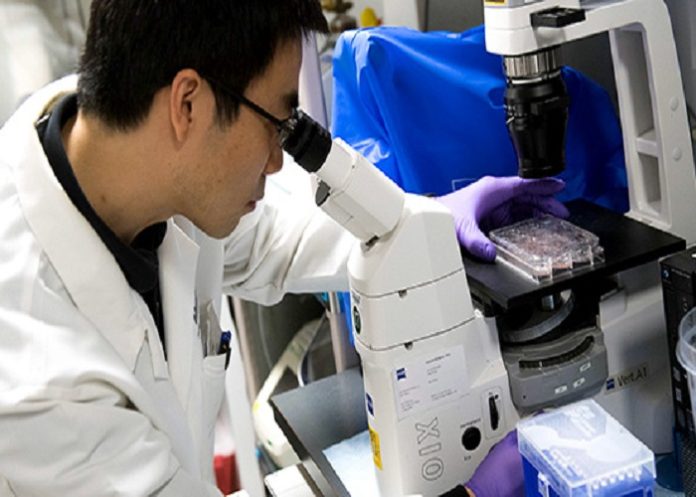
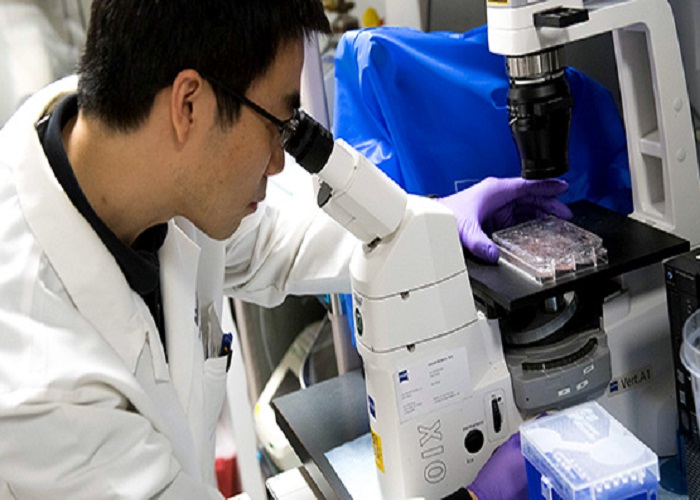
Experimental trials are ongoing at the National Institutes of Health Clinical Center, a US government-funded research hospital where doctors are trying to partially replace patients’ immune systems with T-cells that would specifically attack cancers caused by the human papillomavirus (HPV), a common sexually transmitted infection. A person’s T-cells will naturally try to kill off any invader, including cancer, but usually fall short because tumors can mutate, hide, or simply overpower the immune system.
Immunotherapies that have seen widespread success, such as chimeric antigen receptor (CAR-T) cell therapies, mainly target blood cancers like lymphoma, myeloma and leukemia, which have a tumor antigen — like a flag or a signal — on the surface of the cells so it is easy for immune cells to find and target the harmful cells. But many common cancers lack this clear, surface signal. Hinrichs’ approach focuses on HPV tumors because they contain viral antigens that the immune system can easily recognize.
/ AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images)
कुछ टॉप के वैज्ञानिक और अकादमिक पब्लिशिंग घरानों जैसे एल्सेविअर, विली इंडिया, विली पीरियॉडिकल्स और अमेरिकन केमिकल सोसायटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसा मुकदमा दायर किया है जो भारत के छात्रों तथा शोधार्थियों के हितों पर गहरी चोट करता है। ये प्रकाशक अपने जर्नलों में प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित शोध लेख प्रकाशित करते हैं। लेकिन इन इनकी कीमत इतनी ज्यादा रखी जाती है कि एक साधारण परिवार के बच्चे के लिए इन्हें खरीद पाना असंभव है। साधन संपन्न संस्थाएं और लाइब्रेरियां ही इन्हें खरीदने की क्षमता रखती हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा है कि भारत में साई-हब और लिबजेन नामक वेबसाइटों पर रोक लगाई जाए। महंगे जर्नलों में छपने वाले शोधपत्र इन वेबसाइटों पर सबके लिए सुलभ हैं। उदाहरण के तौर पर, केवल साई-हब वेबसाइट पर विज्ञान से संबंधित 5 करोड़ पेपर्स उपलब्ध हैं और यह संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है।
गैरकानूनी मगर उपयोगी
यह वेबसाइट 2011 में कजाखस्तान की 22 वर्षीया साइंस ग्रैजुएट अलेक्सेंद्रा एल्बाक्यान ने बनाई थी, जो खुद भी साइंस जर्नलों के अनाप-शनाप दामों की भुक्तभोगी थी। उसने दुनिया भर के छात्रों व शोधकर्ताओं के लिए यह वेबसाइट बना दी जो केवल विकासशील देशों में ही नहीं विकसित देशों में भी बहुत पॉप्युलर है। चीन और अमेरिका तक में वैज्ञानिक समुदाय इस वेबसाइट पर बहुत निर्भर हैं। कॉपीराइट के सवाल को लेकर अमेरिकन पब्लिशर्स ने कम से कम दो बार साई-हब के मालिक पर मुकदमा किया है, तब भी यह वेबसाइट चालू है जबकि शुद्ध कॉपीराइट के सवाल पर इसे गैरकानूनी करार दिया गया है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 2016 में केवल भारत में छात्रों तथा शोधार्थियों ने साई-हब वेबसाइट से 70 लाख पेपर डाउनलोड किए। अगर ये पेपर्स इस वेबसाइट पर न मिलते तो उन्हें लगभग 1800 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते। इस रकम को अगर भारत के कुल शोधार्थियों और छात्रों के बीच विभाजित किया जाए तब भी प्रति व्यक्ति यह खर्च लगभग 1 लाख रुपये के आसपास बैठेगा।
वैज्ञानिक जर्नलों के प्रकाशक दलील देते हैं कि कागज, प्रिंटिंग और लेबर का खर्च दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और यह कि उन्हें अपने व्यवसाय के लिए अधिक पैसा चाहिए। इन प्रकाशकों से कोई पूछे कि अगर सचमुच उन्हें घाटा हो रहा है तो उनके कारोबार को दुनिया के सबसे ज्यादा मुनाफे के कारोबारों में क्यों गिना जाता है। एल्सेविअर को लें, जिसका नाम दिल्ली के उक्त मुकदमा दायर करने वाली कंपनियों में एक है, तो इस प्रकाशक का मुनाफा अपने कुल राजस्व का 40 प्रतिशत बैठता है जबकि दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी गूगल का मुनाफा उसके कुल राजस्व का 19 प्रतिशत भी नहीं बैठता। जर्नलों के प्रकाशकों का मसला दरअसल हिंदी के छुटभैये प्रकाशकों से अलग है। रिसर्च करने वाले अधिकतर शोधार्थी सार्वजनिक फंड से अपना काम करते हैं और शोध प्रकाशकों के पास यह धन भी इन्हीं शोधार्थियों से आता है।
अगर कोई शोधार्थी चाहे कि जो काम उसने किया है, वह आम जनता को डिजिटल रूप में यानी मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए, ताकि सबको इससे लाभ मिले, तो इसके लिए उसको अलग से अपनी जेब से प्रकाशक को पैसे देने पड़ते हैं। अब देखिए कि यह धन वैज्ञानिक समुदाय का वह व्यक्ति प्रकाशक को देता है जो विभिन्न प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरियों और दूर-दराज की जगहों पर जाकर, उदाहरण के तौर पर, चमगादड़ों के वायरस का अध्ययन करता है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर किसी वैक्सीन पर काम करता है। तब जाकर तमाम जद्दोजहद के बाद अपने शोध को दुनिया के सामने पेश कर पाता है। इस पूरी यात्रा में प्रकाशक का योगदान जीरो के बराबर ही होता है। इन प्रकाशकों का लगभग 90 प्रतिशत राजस्व इन शोधों की डिजिटल बिक्री से आता है। उसे किताब या जर्नल की शक्ल देने की जरूरत ही नहीं रहती। बड़े-बड़े शहरों में मोटे-मोटे जर्नल रखने की जगह किसके पास होती है!
जाहिर है, ये जर्नल लाइब्रेरियों और संस्थागत शोध अकादमियों की शोभा बढ़ाते हैं। इन वैज्ञानिक जर्नलों के दाम पिछले 30 वर्षों में 6 गुना बढ़ गए हैं जबकि इनमें प्रयुक्त सामग्री का मूल्य सूचकांक सिर्फ 2 गुना हुआ है। साफ है कि प्रकाशकों ने इस ज्ञान पर अपना इजारेदाराना हक हासिल कर लिया है, जिसे चुनौती देने का वक्त आ गया है। यहां एक मशहूर अमेरिकी शोधार्थी एरॉन श्वार्त्ज का जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर अनेक महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर्स डाउनलोड किए थे। उन्हें वे आम जनता के लिए सुलभ कराना चाहते थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जब आभास हुआ कि अमेरिकी कानूनों के अंतर्गत उन्हें लंबी अवधि की जेल हो सकती है तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। ज्ञान को इजारेदारों की कैद से आजाद करने के संघर्ष में यह पहली शहादत थी।
ओपन ऐक्सेस मैनिफेस्टो
2008 में एरॉन श्वार्त्ज ने ‘गुरिल्ला ओपन ऐक्सेस मैनिफेस्टो’ प्रकाशित कराया था जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं, ‘सूचना ताकत है लेकिन जैसा कि हर ताकत के मामले में होता है, कुछ लोग हैं जो उसे अपने हाथों तक सीमित रखना चाहते हैं। दुनिया की समूची वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विरासत, जो सदी दर सदी किताबों तथा जर्नलों के रूप में प्रकाशित होती रही है, बड़े पैमाने पर डिजलीकृत की जा रही है और मुट्ठीभर निजी कारपोरेशनों द्वारा तालाबंद की जा रही है। क्या आप उन प्रपत्रों को पढ़ना चाहेंगे जिनमें विज्ञान के सबसे मशहूर नतीजे प्रस्तुत किए गए थे? यदि हां, तो आप को रोड एल्सेविअर जैसे प्रकाशकों को भारी राशि देनी होगी।’ इसका एक अर्थ यह हुआ कि अमेरिकी जर्नल प्रकाशक भारत में शोधकर्ताओं की राह मुश्किल करना चाहते हैं, जिससे न केवल इन छात्रों का नुकसान होगा बल्कि हमारे देश के एक उदीयमान वैज्ञानिक शक्ति बनने की राह में भी रुकावट पैदा होगी।
अजय कुमार
(लेखक स्तंभकार हैं ये उनके निजी विचार हैं)





















