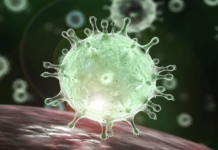देश में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार के नए बजट में कृषि-क्षेत्र को लेकर होने वाली घोषणाओं की ओर सबकी निगाह स्वाभाविक रूप से लगी हुई थी। इस तरह की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के संबंध में हुई है, जो आंदोलन के केंद्रीय विषय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सरकारी खरीद से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि अभी तक एफसीआई को छोटी बचत योजनाओं के फंड (एनएसएसएफ) से जो कर्ज मिलता था, वह बंद किया जा रहा है। यह एफसीआई के गले की नस काटने जैसा है। जाहिर है, इसका दुष्प्रभाव एमएसपी पर होने वाली सरकारी खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) द्वारा देश के 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले सस्ते खाद्यान्न वितरण, दोनों पर पड़ेगा। एफसीआई किसानों से एमएसपी पर खरीद करता है और पीडीएस में सस्ती दर पर गरीबों को देता है। इस क्रम में होने वाले घाटे की भरपाई के लिए सरकार से उसे सब्सिडी मिलने का प्रावधान है लेकिन असलियत में यह सब्सिडी बहुत कम होती है। 2019-20 में एफसीआई को 3 लाख 17 हजार करोड़ सब्सिडी की जरूरत थी, पर उसे मात्र 75 हजार करोड़ की राशि मिली। बाकी पैसा एफसीआई ने सरकार की लघु बचत योजनाओं के फंड से 8 फीसदी ब्याज दर पर उधार लिया। सरकारी सहायता के अभाव में उसका कर्ज लगातार बढ़ते हुए 31 मार्च 2020 तक 2 लाख 54 हजार करोड़ हो गया था। अब जब यह सस्ता कर्ज भी सरकार ने बंद कर दिया है, तो एफसीआई को मंहगी दरों पर बाजार से ऋण लेना पड़ेगा।
इसके चलते कर्ज में डूबते एफसीआई द्वारा एमएसपी पर की जाने वाली खरीद कम से कमतर होती जाएगी, जो अंतत: समूची एमएसपी-पीडीएस व्यवस्था को खात्मे की ओर ले जाएगी। किसान आंदोलन के सबसे बुनियादी प्रश्न पर बजट में इस विपरीत घोषणा से सरकार ने आंदोलन के प्रति अपने रुख और दिशा का ऐलान कर दिया है। तीनों कृषि कानूनों के पीछे सरकार की मंशा को लेकर किसान नेताओं द्वारा व्यक्त की जा रही आशंकाओं को इस घोषणा ने सही साबित किया है। इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा, पर इसके तीन संभावित राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। पहला यह कि मोदी सरकार इससे लगे झटके को झेल जाए। दूसरा, इससे पैदा हुए विक्षोभ का फायदा उठाते हुए विपक्ष 2024 में बीजेपी को हराकर साा में वापसी कर ले। एक तीसरी संभावना भी है कि भारतीय इतिहास के इस अभूतपूर्व आंदोलन के गर्भ से एक नई राजनीति का जन्म हो, जो आने वाले दिनों में देश के समूचे राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करे। समझना होगा कि अन्य विशेषताओं के साथ-साथ रैडिकल अंतर्वस्तु की दृष्टि से भी यह आंदोलन भारतीय जनांदोलनों के इतिहास में अनूठा है। पहले के आंदोलन आंशिक मांगों पर आधारित होते थे। कभी राजनीतिक तो कभी कोरे अर्थवादी। उनका अपना स्वतंत्र वैचारिक-राजनीतिक आयाम नहीं विकसित होता था। चुनाव आते-आते वे आराम से पक्ष या विपक्ष की जनविरोधी राजनीति द्वारा इस्तेमाल हो जाते थे। लेकिन मौजूदा आंदोलन मुद्दा आधारित होने के बावजूद अर्थनीति के बुनियादी सवालों से टकरा रहा है।
इस आंदोलन ने अमूर्त राष्ट्रवाद के डॉमिनेंट नैरेटिव को चुनौती दी है। सरकार पहले कृषि कानूनों को किसान हित में बता रही थी, पर किसान जब अपने हितों के आधिकारिक प्रवक्ता बनकर स्वयं सामने आ गए, तब सरकार किन्हीं अमूर्त राष्ट्रीय हितों का हवाला दे रही है। अब ये रहस्यमय राष्ट्रीय हित क्या हैं? अगर यह किसानों का हित नहीं है, गरीब और मध्यवर्गीय जनता का हित नहीं है तो फिर किसका हित है? कौन है राष्ट्र? क्या कॉरपोरेट हित ही राष्ट्रहित है? क्या कॉरपोरेट ही राष्ट्र है? 26 जनवरी के घटनाक्रम के बाद किसान आंदोलन को राष्ट्रद्रोही बताकर कुचलने की कोशिश परवान न चढ़ सकी। गद्दार प्रचारित किए जाने से आक्रोशित किसान दुगुने आवेग के साथ उठ खड़े हुए हैं। किसान आंदोलन ने यह भी दिखा दिया कि कारपोरेट हित को राष्ट्रीय हित बताने वाला राष्ट्रवाद का मॉडल विभाजनकारी है। आंदोलन को बदनाम करने, बांटने और तोडऩे के लिए इसके लाड़ले राष्ट्रीय एकता को दांव पर लगाने में भी कोई संकोच नहीं करते। क्या-क्या नहीं कहा गया किसानों को?
खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े-टुकड़े गैंग। यही नहीं, पंजाब के खिलाफ हरियाणा वालों को खड़ा करने की कोशिश की गई। फिर पंजाब-हरियाणा वालों के खिलाफ पूरे देश को खड़ा करने का अभियान चलाया गया। शाहीन बाग के जरिए मुस्लिम विरोधी भावना का भी आंदोलन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हुई। इस सबके बावजूद किसान आंदोलन क्षेत्र/ धर्म/ जाति/ लिंग/ आर्थिक विभेदीकरण की सीमाएं पार करता हुआ समावेशी राष्ट्रीय एकता का मंच बन गया। किसान आंदोलन ने लोकतंत्र के प्रश्न को नई ऊंचाई दी है। जनता के जीवन को लोकतंत्र की बुनियादी कसौटी बनाते हुए उसने विरोध के संवैधानिक अधिकार को सर्वोच्चता प्रदान की है। किसानों ने भागीदारी मूलक लोकतंत्र का सवाल खड़ा किया है कि या बिना उनकी राय लिए सरकार कोई भी कानून बनाकर उनपर थोप सकती है? उन्होंने इस बुनियादी लोकतांत्रिक उसूल को बुलंद किया है कि चुनाव जीत जाने से किसी को पांच साल मनमानी करने का निरंकुश अधिकार नहीं मिल जाता।
लाल बहादुर सिंह
( लेखक छात्र नेता हैं ये उनके निजी विचार हैं)