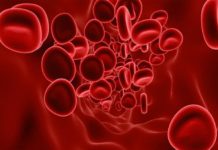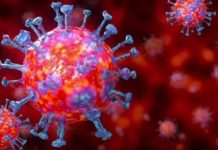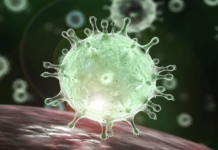केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के पुलिस थानों की रैकिंग के लिए शुरू की गई प्रक्रिया से पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार की नई उम्मीद जागी है। वैसे तो 2017 में भी कुछ इसी तरह की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन इस बार की पहलकदमी इस मायने में विशिष्ट मानी जा रही है कि इसमें देश भर के थानों को सात मानदंड़ो के आधार पर जांचा-परखा जा रहा है। निरंतर बढ़ रहे अपराधों की रोक थाम के लिए उठाए गए अभिनव कदमों और जनता के फीडबैक को इसके केंद्र में रखा गया है। इससे एक स्वस्थ प्रतियोगिता शुरू होने की संभावना है। थाने अपना रेकॉर्ड बेहतर दिखाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कानून-व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी के लिए पुलिस को दोष देने का चलन पुराना है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि पुलिस की स्थापना ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी।
दिक्कत यह है कि आज भी हमारी पुलिस प्रणाली बहुत कुछ 1861 के पुलिस ऐक्ट के हिसाब से चल रही है, जिसका मक सद 1947 से पहले कुछ और था। आजादी के बाद भी काफी समय तक इन औपनिवेशिक तौर- तरीकों का चलन रहा। बीच-बीच में बदली परिस्थितियों के मद्देनजर तत्कालीन पुलिस नेतृत्व द्वारा औपनिवेशिक कार्यप्रणाली को लोक तांत्रिक बनाने की कोशिशें भी होती रहीं। देश के प्रबुद्ध तबके द्वारा पुलिस सुधारों की मांग उठाई जाती रही लेकिन इस दिशा में कुछ खास हुआ नहीं क्योंकि सत्ताधारी वर्ग ने इस कार्यशैली को अपने लिए उपयुक्त पाया। 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद के दो वर्षों में पुलिस की कार्रवाइयों ने जनमानस में औपनिवेशिक पुलिस की यादें फिर ताजा कर दीं।
पुरानी पीढ़ी तो वह सब अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भुगत ही चुकी थी, अब नई पीढ़ी को भी वही सब झेलना पड़ा। इसलिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व आईसीएस धर्मवीर की अध्यक्षता में 15 नवंबर 1977 को पुलिस प्रणाली में आमूल परिवर्तन के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया। आयोग ने पूरी शिद्दत से 1981 तक कुल 8 रिपोर्टें सरकार को सौंपीं, लेकिन इन पर खास अमल नहीं हुआ। 1980 में कांग्रेस के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद इस आयोग का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। लेकिन आयोग के प्रयासों ने पुलिस सुधार को एक बड़ा अजेंडा बना दिया। सरकार भी कुछ कम महत्वपूर्ण सिफारिशें मानने को राजी हो गई, जिनसे पुलिस कार्यप्रणाली में केवल सांकेतिक बदलाव ही आ पाया। फिर भी देश में पुलिस सुधारों की नींव पड़ गई और इनकी बातें जोर-शोर से होने लगीं। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस जूलियस रिबेरो की अगुआई में समिति बनाकर उसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों और नए पुलिस कानून के मसौदे पर काम करने को कहा।
2000 में पूर्व गृहसचिव पद्मनाभन के नेतृत्व में एक और समिति बनाकर पुलिस में बढ़ता राजनीतिकरण और अपराधीकरण रोकने तथा इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया। 2005 में गठित पुलिस प्रारूप समिति ने 1861 के पुलिस ऐक्ट की जगह एक मॉडल पुलिस ऐक्ट की पेशक श की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कुछ निर्देश भी दिए। 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस संबंध में कुछ सुझाव दिए। इनके अलावा छिटपुट प्रयासों की फेहरिस्त भी लंबी है। लेकिन अभी तक कुछ खास हो नहीं पाया। मौजूदा स्थिति यह है कि जहां संयुक्त राष्ट्र प्रति एक लाख की आबादी पर 222-230 पुलिसकर्मियों की बात करता है वहीं भारत में यह उपलब्धता 2014 में 125, 2016 में 138 और 2017 में 144 तक ही पहुंच पाई। 2013 में पुलिसकर्मियों के देश में स्वीकृत 22.8 लाख पदों में भी 25 प्रतिशत खाली थे। जनवरी 2018 आते-आते स्थिति में कुछ सुधार हुआ और स्वीकृत पदों की संख्या 23,79,728 हुई।
लेकिन कार्य करने के लिए पुलिसकर्मियों की उपलब्धता अभी भी 18,51,332 ही रही, क्योंकि गृह मंत्रालय के मुताबिक रिक्तियां 5,28,396 हैं। अनुमान है कि यदि इन खाली पदों को भर दिया जाए तो भी प्रति एक लाख जनसंख्या को 185 पुलिसकर्मी ही मिल पाएंगे। सबसे ज्यादा रिक्तियां उत्तर प्रदेश में 1,28,952, बिहार में 50,291, पश्चिम बंगाल में 48,981 और तेलंगाना में 30,345 हैं। इसके चलते इन राज्यों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और प्रति लाख आबादी के लिए यहां पुलिसक र्मी उपलब्ता 100 से भी कम है। हां, जम्मू कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों और पंजाब में यह 500 के पार है, जिसके अलग कारण हैं। पुलिस के लिए उपलब्ध संसाधनों का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। राज्य सूची का विषय होने के कारण पुलिस के लिए संसाधनों की व्यवस्था राज्य सरकारों को ही करनी होती हैं। औसत रूप से देखें तो 2011-15 के बीच पुलिस पर राज्य बजट का 4.4 प्रतिशत खर्च होता था।
जो अभी कहीं-कहीं तो घटक र 3 से 4 प्रतिशत ही रह गया है। इसका सीधा असर आवश्यक हथियारों, उपकरणों और वाहनों पर देखा जा सकता है। पुलिस की इस स्थिति के लिए अन्य सरकारी विभागों की तरह स्वयं पुलिस विभाग और इसकी कार्य संस्कृति बराबर की जिम्मेदार है। बदलता नजरिया वैश्वीकरण और सूचना तकनीक के मौजूदा दौर में देश की जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुकी है और अन्य देशों की तर्ज पर वह पुलिस से ज्यादा अपेक्षाएं भी रखने लगी है। इन अपेक्षाओं पर खरा न उतरने की स्थिति में पुलिस पर उसका गुस्सा जाहिर होने लगा है। एक लोक तांत्रिक देश में कोई बड़ा परिवर्तन बिना राजनीतिक इच्छाशक्ति के असंभव है। पुलिस कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन भी इसके बिना नहीं हो सकता। वैसे भी आर्थिक सुधारों और विदेशी पूंजी निवेश के लिए कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ होना पूर्व शर्त जैसा है। राजनीतिक नेतृत्व को यह बात समझनी होगी।
महेश भारद्वाज
(लेखक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, ये उनके निजी विचार हैं।)