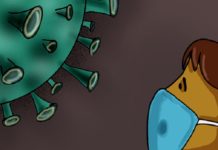हमारे ये पूर्व-हमजोली पुलिस के बड़े अफ़सर हुआ करते थे। एक इज़्जतदार औद्योगिक घराने का स्नेह भी उन पर रहा है। दक्षिण भारत के हैं, मगर बिहार-झारखंड को झन्नाटेदार पुलिस-सेवा देने के लिए जाने जाते रहे। उनकी सिंघमगीरी पर ‘सिंघम’ से भी आठ साल पहले 2003 में बंबई फिल्म जगत ने, कहते हैं कि, ‘गंगाजल’ बनाई थी। बिहार से अलग हो कर झारखंड बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी। हमारे मित्रवर ने जन-सेवा के लिए पुलिस-सेवा छोड़ दी और मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा में शरीक हो गए।
बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की सेवा में रत हो गए मरांडी में उन दिनों हमारे मित्र को ज़रूर कुछ दिखा होगा। मरांडी की पार्टी तब तक दो-फाड़ हो गई थी। मित्र मरांडी की बांह थाम कर एक उपचुनाव के ज़रिए 2011 में लोकसभा पहुंच गए। वे भाजपा के उम्मीदवार को डेढ़ लाख वोट से हरा कर आए थे। मगर 2014 का चुनाव हुआ तो एक लाख वोट से हार गए। ऐसे में उनका मरांडी से मोह-भंग हो गया। सो, बावजूद इसके कि कांग्रेस की बहुत बुरी गत हो गई थी, या फिर इसीलिए कि बुरे वक़्त में कांग्रेस के भीतर पैठ बनाना ज़्यादा आसान होगा, वे कांग्रेस में आ गए। आते ही पार्टी के प्रवक्ता बन गए। और, सच कहूं, प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने कारगर काम किया।
फिर राहुल गांधी ने हमारे मित्रवर को झारखंड की कांग्रेस का मुखिया बना दिया। लोगों ने कहा कि जुम्मा-जुम्मा तीन साल पहले पार्टी में आए व्यक्ति को इतनी अहम ज़िम्मेदारी देना ठीक नहीं होगा, कि कर्नाटक का आदमी झारखंड को कैसे संभालेगा, कि प्रशासनिक सेवा की कुलीन जीवन शैली में रचे-बसे व्यक्ति को एक आदिवासी राज्य का संगठन सौंपना कौन-सी बुद्धिमानी है; मगर राहुल ने ये सारी दलीलें किनारे कर दीं और हमारे मित्र के मस्तक पर अपने परम-विश्वास की मुहर लगा दी। 2019 में कांग्रेस की हार के बाद जब राहुल ने जवाबदेही का मसला उठा कर पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा तो हमारे मित्रवर उन लोगों में थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने को इस उत्तरदायित्व से नत्थी किया और प्रदेश-अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दे दिया।
हालांकि कई औरों ने भी दिखाने को इस्तीफ़े दिए, लेकिन सब जानते हैं कि बाकी बहुत-से राहुल का साथ देने में बगलें झांक रहे थे। ऐसे में मित्रवर को साथ खड़े देख कर मुझे भी औरों की तरह ख़ुशी हुई। राहुल तो अपने इस्तीफ़े पर अड़े रहे, मगर उनके जाते ही ज़्यादातर हाथियों ने अपने दिखाने के दांत निपोरना भुला दिया और अपनी-अपनी कुर्सियों से फिर चिपट गए। मौक़ा था, सो, ताक में बैठे झारखंडी खांटियों ने बिसात बिछाई और हमारे मित्र की जगह दूसरे की नियुक्ति हो गई।
ये मित्र पुदुचेरी के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए थे। उन्होंने निजी कॉरपारेट जगत में भी काम किया। वे मरांडी-नुमा राजनीति का अनुभव भी रखते थे। कांग्रेस के खो-खो के खेल की बारीकियां भी उनसे कौन-सी छिपी रह गई थीं? इतने पर भी वे अपने दिल की धड़कनों की लय बना कर नहीं रख पाए और बेसबरे की तरह सिसोदिया के सामने नत-मस्तक हो गए। वैकल्पिक राजनीति के जुमलेबाज़ों से तो कांग्रेस में ही उनकी प्रतिभा का बेहतर उपयोग होता। झारखंड के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चार-छह सीटें कबाड़ लेने के बाद सत्ता की तराजू के संतुलन का खेल खेलने की उम्मीद रखने की अल्पकालिक सियासी लक्ष्य के चक्कर में अपनी डाल काट लेने की बुद्धि पर तरस खाने के अलावा क्या करें?
मित्र कोई ऐसे भी लंगोटिया नहीं थे कि मैं हाय-हाय करूं। उनका जाना कोई ऐसी घटना भी नहीं है कि बाबू जगजीवनराम ऐन वक़्त पर रामलीला मैदान पहुंच गए हों या प्रणव मुखर्जी ने अपनी पार्टी बना ली हो या शरद पवार ने कांग्रेस से विदा ले ली हो। फिर भी मैं इस प्रसंग पर इतने आंसू क्यों बहा रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मित्र भले ही ज़्यादा वज़नदार न हों, मगर उनके जाने की कथा आज की कांग्रेस की असली व्यथा है। इस व्यथा-कथा को समझे बिना कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। कांग्रेस को व्यक्तियों के नहीं, प्रवृत्तियों के प्रश्न का समाधान खोजना है। उसे अपनी सांगठनिक मनःस्थिति और मंझले कर्णधारों की ग्रंथियों का हल निकालना है।
इस मित्र ने मेरे ट्वीट के जवाब में लिखा कि उन्हें राहुल गांधी से कोई शिकायत नहीं है। मैं भी जानता हूं कि उन्हें झारखंड के टंटेबाज़ों से परेशानी थी, राहुल से नहीं। लेकिन कांग्रेसी राजनीति की गलियों का आवारा राही होने के नाते मैं समझना चाहता हूं कि यह तो ठीक है कि जिन्हें राहुल के रहते अपना भविष्य नज़र नहीं आया, वे छोड़ कर चले गए, मगर आख़िर कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है कि जिनका भविष्य राहुल की वजह से बना और आगे भी बनता, वे भी छोड़ कर जा रहे हैं?
फिर ऐसे लोग भी तो कम नहीं हैं, जिन्हें राहुल-टोली ने ठिकाने लगाने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी और वे फिर भी पार्टी छोड़ कर नहीं गए। सवाल है कि छोड़ कर जा रहे लोग क्यों इतने निराश हैं? नहीं जा रहे लोग किस उम्मीद क्यों और किस उम्मीद से बंधे हैं? यह किसी वैचारिक द्वंद्व का दौर है या सिर्फ़ निजी आकांक्षाओं की पूर्ति का युग? अपने ही हमजोलियों से रोज़-रोज़ का अपमान झेलने के बावजूद जो डटे हैं, क्या वे महज़ वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण जमे हुए हैं? क्या जो विदा ले रहे हैं, सिर्फ़ अपनी इच्छाएं भर पूरी करना चाहते हैं?
इस भंवर की गुत्थी को समझ कर सुलझाने का दायित्व-बोध अगर कांग्रेस के एवरेस्ट पर बैठे समूह में होगा तो कांग्रेस बच जाएगी। अब भी जिन्हें त्वरित निर्णयों की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, वे किन चप्पुओं के सहारे पार जाने को सोच रहे हैं? राजनीतिक संगठन पिछले जन्मों के पुण्यों के भरोसे ही नहीं चलते। उन्हें चलाने के लिए इस जन्म में भी अनवरत साधना करनी होती है। इस साधना में आने वाला अंतराल सारे किए-कराए पर पानी फेर देता है। सियासत निराकार-ऊर्जा से संचालित होने वाली सृष्टि-रचना नहीं है। वह भौतिक-जगत का ऐसा स्थूल स्वरूप है, जिसके वाहक को स-शरीर और स-विवेक हर लमहे इस झंझावात में मौजूद रहना होता है। जो रह पाते हैं, वे अपनी पताका फहराते हैं। जो नहीं रह पाते हैं, स्मृति-शेष हो जाते हैं।
पंकज शर्मा
(लेखक न्यूज़-व्यूज़ इंडिया के संपादक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।)