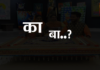भारतीय विदेश नीति एक बार फिर चक्रव्यूह में उलझी है। पड़ोसी राष्ट्रों, यूरोप तथा पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में जिस तरह के विरोधाभासी हालात बन रहे हैं, वे इस बात पर जोर देते हैं कि आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियों से कहीं अधिक परदेसी नीतियों के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। हिन्दुस्तान के भीतर तो उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और यह देश काफी हद तक उनसे निपटने में भी सक्षम है। लेकिन वैदेशिक संबंधों के बारे में बेहद जिम्मेदार और जवाबदेह होने की आवश्यकता है। यदि इसे काम चलाऊ ढंग से लिया गया तो वैश्विक परिदृश्य में आने वाले दिन मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उनके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका और सहयोगी देशों के सैनिकों की वापसी के बाद इस मुल्क का भविष्य खतरनाक संकेत दे रहा है। दो राय नहीं कि तालिबान अब वहां अधिक ताकतवर और विराट आकार में प्रस्तुत होंगे। अफगानी सरकार उनका कब तक मुकाबला कर सकेगी-कहना कठिन है। बीस-पच्चीस बरस पहले उन्हें उग्रवादी कहा जा सकता था, पर अब इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
वे अफगानिस्तान में अनुदार विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसके आगे उदारवादी समर्पण करते दिखाई देने लगे हैं। कमोबेश यही स्थिति दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम राष्ट्रों की है। उदार और मुत द्वार की नीति के चहेते हाशिये पर हैं। विडंबना यह कि यह विचारधारा वामपंथियों की उस सोच का समर्थन करती है कि बंदूक की नली से सत्ता की गली मिलती है। विचार के धरातल पर इस तरह के लोग साथ-साथ खड़े नजर आते हैं। दक्षिण एशिया के अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। दूसरी श्रेणी वह है जहां लोकतांत्रिक मुखौटे के साथ अधिनायक पनप चुके हैं। चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान ऐसे ही देश हैं। तो इसका या अर्थ लगाया जाए कि तेज गति से भागते मौजूदा संसार की दिलचस्पी अब शासन प्रणालियों में या कहा जाए कि जम्हूरियत में नहीं रही है। एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि आम नागरिक को सामूहिक नेतृत्व-शासन शैली से कोई खास लगाव नहीं रहा है। यानी कि तानाशाही से भी उसे ऐतराज नहीं है। अपवादों को छोड़ दें तो वह अब अपने अधिकारों के लिए लडऩा नहीं चाहता।
लोकतांत्रिक हिन्दुस्तान अब तक तालिबान के साथ सीधे संवाद से बचता रहा है। लेकिन जब लोकतांत्रिक अमेरिका तालिबान से समझौते पर उतर आया तो हिन्दुस्तान के लिए भी झिझक यों होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी सैनिकों की वापसी चाहते थे और जो बाइडेन भी। जाहिर है यह देश की मांग थी। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत का भारी पूंजीनिवेश दांव पर है। ईरान में चाबहार बंदरगाह के जरिये अफगानिस्तान से व्यापार की संभावनाओं पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद उनका भारत के साथ कैसा व्यवहार रहेगा। पिछली पारी में उनकी प्राथमिकता मजहबी रही है। पर अब तालिबानी नेतृत्व भी वह नहीं रहा है। हमें आशा करनी चाहिए कि उनकी अल पर पड़े पर्दे हट चुके होंगे। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी विदेश नीति में लचीलापन तो लाना ही होगा। एक कारण यह भी है कि भारत नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान का रुतबा बढ़े और उसकी दशकों की पूंजी लूट ली जाए।
याद रखना चाहिए कि जब पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर सैनिक शासन लगाया था तो हिन्दुस्तान ने ऐलान किया था कि वह पाकिस्तान में फौजी हुकूमत से कोई संवाद नहीं करेगा, पर वही मुशर्रफ सम्मान से आगरा शिखर वार्ता में आए थे। इसलिए एक बार फिर तालिबान के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल करने के लिए यू-टर्न लेना पड़े तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है कि इमरान सरकार से तालिबान भी सहज नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका-तालिबान समझौते के बाद गाल बजाए हैं और भारत को दूर रखने की बिन मांगी सलाह तालिबान को दी है, वह उन्हें रास नहीं आई है। इमरान हुकूमत तो यहां तक कह चुकी है कि वे तालिबान सरकार को पसंद ही नहीं करेंगे।
तालिबान के आने की आशंका से चीन भी कम परेशान नहीं है। उसे लगता है कि तालिबान शिनजियांग प्रांत में आजादी का समर्थन कर सकते हैं और उईगर मुस्लिम उग्रवादी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खनिजों के उत्खनन में उसका पूंजी निवेश भी डूबने की आशंका है। चीन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन आर्थिक झटके नहीं। पाकिस्तान में पहले ही उसका बहुत पैसा डूब चुका है। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान में रौब की स्थिति बनानी चाहिए। याद रखिए कि इस खूबसूरत पहाड़ी मुल्क से हिन्दुस्तान के सदियों पुराने आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते रहे हैं। उनकी उपेक्षा ठीक नहीं है।
राजेश बादल
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं ये उनके निजी विचार हैं)